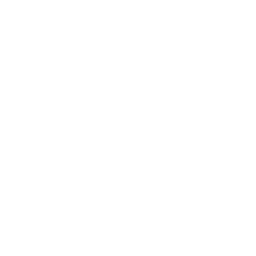राजनीतिक हित साधने का जरिया न बने भाषा
किसी अफसर को राज्य-विशेष की भाषा बोलनी नहीं आती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सरेआम थप्पड़ मार दिया जाये। भाषा के हित साधने का यह तरीका अनुचित ही नहीं, आपराधिक भी है। उचित तरीका तो यह है कि हम अपनी भाषा को इतना समृद्ध बनायें कि हर किसी को उसे सीखने, काम में लेने की इच्छा होने लगे।

महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी को मराठी न बोल पाने की सज़ा भुगतनी पड़ी। मातृभाषा मराठी के प्रति अतिरिक्त लगाव वाले कुछ मराठी युवाओं ने यह सज़ा दी थी। उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का संरक्षण प्राप्त था। अब मनसे के नेता राज ठाकरे ने अपने अनुयायियों से कह दिया है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने की अनिवार्यता के लिए अभियान जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। लोग समझ गये हैं। लोग कितना समझे हैं, और राज्य में मराठी भाषा का उपयोग कितना बढ़ जायेगा, यह तो आने वाला कल ही बतायेगा, लेकिन यह बात तो सहज समझ में आने वाली है कि जो जहां रह रहा है, उसे क्षेत्र-विशेष की भाषा तो आनी ही चाहिए। लेकिन यहीं इस बात की समझ की भी अपेक्षा की जाती है कि हमारा संविधान रोजी-रोटी के लिए कहीं भी आने-जाने, बसने का अधिकार देश के हर नागरिक को देता है। आसेतु-हिमालय सारा भारत देश के सब नागरिकों का है, सबको कहीं भी जाकर बसने का अधिकार है। ऐसे में, क्षेत्र-विशेष की भाषा बोलने की शर्त हर नागरिक के लिए लागू करना शायद उतना व्यावहारिक नहीं होगा, जितना समझा जा रहा है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई भाषा न बोल पाने वाला उस भाषा के प्रति अवमानना का भाव रखता है।
यहीं इस बात को रेखांकित किया जाना ज़रूरी है कि अपनी भाषा के प्रति लगाव का भाव होना एक स्वाभाविक स्थिति है, अपनी भाषा के प्रति प्यार और सम्मान का भाव होना ही चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम देश की अन्य भाषाओं के प्रति अवमानना का भाव रखें। देश की सारी भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, और हमें सब पर गर्व होना चाहिए।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न भाषाओं से समृद्ध हमारे भारत में भाषा के नाम पर विवाद खड़े किये जाते हैं। इस मुद्दे पर कई बार विभिन्न राज्यों में हिंसक घटनाएं भी हो चुकी हैं। उस स्थिति का मुख्य कारण भाषा को राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति का माध्यम बनाना है। यह एक हकीकत है कि भाषा की इस राजनीति ने देश के अलग-अलग हिस्सों में अप्रिय स्थितियां पैदा की हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों में हमने इस राजनीति के दुष्परिणाम देखे हैं। अब भी समय-समय पर इन दुष्परिणामों की चिंगारियां भड़क उठती हैं।
बहरहाल, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है भाषाई आंदोलन यहां के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मराठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के नाम पर, मराठी अस्मिता की दुहाई देकर राजनीतिक दलों का गठन तक हुआ है। मराठी मानुष के हितों का नाम लेकर राज्य में समय-समय पर आंदोलन होते रहे हैं। इस संदर्भ में ‘मनसे’ की हाल की कार्रवाई ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाली है।
हमारे देश में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ है। ये भाषाएं हमारी कमज़ोरी नहीं, ताकत हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी हर भाषा निरंतर समृद्धि की दिशा में बढ़े, बढ़ती रहे। भाषा के विकास का मतलब यही नहीं है कि उसका विस्तार कितना हो गया है अथवा उस भाषा के बोलने वालों की संख्या कितनी बढ़ गयी है। भाषा के विकास का अर्थ यह भी है कि भाषा की क्षमता कितनी बढ़ी है अर्थात नये-नये विषयों को समझने-समझाने में भाषा कितनी सक्षम हो गयी है या होती जा रही है। साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई भाषा कितनी समृद्ध है, यही तथ्य उसके विकास का असली पैमाना है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज भाषा के नाम पर जो आंदोलन-अभियान चलाये जा रहे हैं उनके पीछे असली मकसद भाषा की समृद्धि नहीं, राजनीतिक हितों को साधने की हवस है। यहां हितों के बजाय स्वार्थ कहना अधिक उपयुक्त होगा। किसी अफसर को राज्य-विशेष की भाषा बोलनी नहीं आती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सरेआम थप्पड़ मार दिया जाये। भाषा के हित साधने का यह तरीका अनुचित ही नहीं, आपराधिक भी है। उचित तरीका तो यह है कि हम अपनी भाषा को इतना समृद्ध बनायें कि हर किसी को उसे सीखने, काम में लेने की इच्छा होने लगे।
लेकिन हमारे यहां स्थित उल्टी है। तमिलनाडु वाले कहते हैं कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है, कर्नाटक वालों को सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी में जानकारी दिये जाने पर ऐतराज है। महाराष्ट्र वालों को शिकायत है कि उनकी भाषा को ‘क्लासिकल दर्जा’ दिये जाने के बावजूद वह सम्मान नहीं दिया जा रहा जिसकी वह अधिकारी है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इन सब के पीछे भाषा विशेष के प्रति प्यार या सम्मान का भाव नहीं होता, अक्सर राजनीतिक स्वार्थ ही इसका कारण बनते हैं ।
यदि बात सिर्फ प्यार या सम्मान की ही है तो राज ठाकरे की चिंता राज्य में मराठी माध्यम के स्कूलों की संख्या का घटना होती। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दस साल पहले की तुलना में मराठी माध्यम के स्कूल आज कहीं कम हैं। वर्ष 2014-15 में मुंबई महानगर पालिका मराठी माध्यम के 368 स्कूल चलाती थी, आज ऐसे सिर्फ 262 स्कूल हैं– अर्थात दस वर्षों में मराठी माध्यम की सौं शालाएं बंद हो गयी हैं! चिंता इस कमी पर होनी चाहिए। पर कोई नहीं पूछ रहा कि यह सौ स्कूल क्यों बंद हो गये। यह तो पूछा जा रहा है कि राज्य में फलां अफसर को मराठी बोलनी क्यों नहीं आती, यह कोई नहीं पूछ रहा कि मराठी माणुस अपने बच्चों को मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना क्यों पसंद नहीं कर रहा? अपनी भाषा के प्रति प्यार और सम्मान के भाव का यह भी एक मतलब है कि हम उसकी क्षमता में विश्वास रखें। अपनी भाषा बोलने-लिखने में गर्व का अनुभव हो हमें।
हाल ही में देश की राजधानी में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्ष डा. तारा भावलकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मराठी भाषा की इसी स्थिति पर चिंता प्रकट की थी। उन्होंने कहा था, ‘हम मराठियों ने अपनी भाषा के ‘क्लासिकल भाषा’ का दर्जा दिये जाने का अभियान चलाया था, और उसे प्राप्त भी कर लिया। हमारी अपेक्षा है कि मराठी निरंतर विकसित हो। पर और भी कई बातें हैं जिनकी हमें चिंता होनी चाहिए।’ इन ‘बातों’ में उन्होंने मराठी में शिक्षा की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, ‘आज मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं और उनकी संपत्ति बेची जा रही है!’
महाराष्ट्र के किसी सरकारी अधिकारी का मराठी बोल पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी यह बात कि महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी भाषा और साहित्य के प्रति कितना आदर-भाव रखते हैं। अपनी भाषा की क्षमता में विश्वास का एक पैमाना यह भी है कि हमारे शिक्षण-संस्थानों में मराठी भाषा में क्या और कितना पढ़ाया जा रहा है; हम में से कितने गर्व से यह कह सकते हैं कि मेरे बच्चे मराठी या गुजराती या बांग्ला या कन्नड़… माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं? आज तो स्थिति यह है कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के गांव-खेड़े तक में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गये हैं और उनके साथ यह जोड़ा जाना भी ज़रूरी हो गया है कि यह ‘इंटरनेशनल स्कूल’ है! इस इंटरनेशनल का क्या मतलब है, मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि आज़ादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अंग्रेजी के गुलाम हो गये हैं। यह बीमार मानसिकता है। इससे उबरना ही होगा।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।