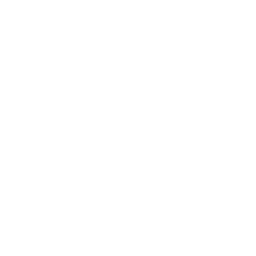कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दिखाई राह
राज्यपाल का पद अगर लोकतंत्र के सहायक संरक्षक की भूमिका निभाए, तो वह उपयोगी हो सकता है, लेकिन जब वह केंद्र सरकार का राजनीतिक उपकरण बन जाता है, तब वह पद संविधान की आत्मा के विरुद्ध चला जाता है।
जयसिंह रावत
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल, 2025 को दिया गया निर्णय भारतीय संघीय ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते, उन्हें या तो मंजूरी देनी होगी, असहमति के साथ लौटाना होगा, या राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। यह निर्णय केवल एक कानूनी निर्देश नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों के लिए एक स्पष्ट ‘लक्ष्मण रेखा’ खींच देने जैसा है, जिससे बाहर जाना अब संविधान की आत्मा के विरुद्ध माना जाएगा। तमिलनाडु प्रकरण और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने केवल एक संवैधानिक संकट का समाधान नहीं किया, बल्कि एक बुनियादी सवाल भी खड़ा किया है। लोकतांत्रिक भारत में राज्यपाल की प्रासंगिकता।
राज्यपाल का पद अगर लोकतंत्र के सहायक संरक्षक की भूमिका निभाए, तो वह उपयोगी हो सकता है, लेकिन जब वह केंद्र सरकार का राजनीतिक उपकरण बन जाता है, तब यह पद संविधान की आत्मा के विरुद्ध चला जाता है। आज का युग जन-जागरूकता और जवाबदेही का है। अब समय आ गया है कि हम यह मूल्यांकन करें कि क्या वाकई राज्यपाल का पद भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत कर रहा है? तमिलनाडु में राज्यपाल रवि ने राज्य सरकार द्वारा पारित 12 विधेयकों को महीनों तक रोके रखा, जिनमें से कई को बिना कारण बताए राष्ट्रपति के पास भेज दिया और कुछ को लौटाया भी। उन्होंने सदन के अभिभाषण के दौरान सरकार द्वारा तैयार भाषण को अधूरा पढ़ा और बीच में ही वॉकआउट कर दिया। ये सभी घटनाएं संविधान की भावना और राज्यों की स्वायत्तता के खिलाफ मानी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इन कृत्यों को ‘लोकतंत्र की उपेक्षा’ बताया और स्पष्ट किया कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है।
यह कोई पहली घटना नहीं है जब राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव सामने आया हो। उत्तराखंड में 2016 में बहुमत परीक्षण से पहले राष्ट्रपति शासन लागू कराना, महाराष्ट्र में 2019 में तड़के सरकार बनवाना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में असंवैधानिक हस्तक्षेप, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में राज्यपालों द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह की उपेक्षा। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि राज्यपाल का पद बार-बार विवादों में रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे रोमेश भंडारी ने 1998 में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की थी, जिसे बाद में न्यायपालिका ने असंवैधानिक करार दिया। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे रामलाल, जो पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ने 1984 में एन.टी. रामाराव की निर्वाचित सरकार को हटा दिया और केंद्र के समर्थन से विपक्षी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इस निर्णय के खिलाफ जनांदोलन खड़ा हुआ, जिसे अंततः राष्ट्रपति को पलटना पड़ा।
राज्यपाल के पद को लेकर संविधान सभा में भी गहन बहस हुई थी। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल केवल ‘संवैधानिक प्रमुख’ होंगे और वे अपनी व्यक्तिगत राय से नहीं, बल्कि राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। कुछ सदस्यों ने यह चिंता भी जताई थी कि राज्यपाल कहीं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनकर राज्यों की स्वायत्तता को बाधित न करे। लेकिन यह माना गया कि अगर पद का उपयोग संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर हो, तो यह संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को ‘नामित प्रमुख’ के रूप में देखा था एक ऐसा पद जो केवल सलाहकार भूमिका निभाएगा, और राज्य की चुनी हुई सरकार की सिफारिशों पर ही कार्य करेगा। परन्तु आज की स्थिति देखें, तो साफ प्रतीत होता है कि राज्यपाल कई बार संविधान निर्माताओं की उस भावना से विचलित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बार-बार दखल देना पड़ रहा है, जो इस व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है।
नि:संदेह, यदि राज्यपाल की भूमिका बार-बार अलोकतांत्रिक साबित होती रहे, तो इसके विकल्पों या इस पद की समाप्ति पर गंभीर विचार जरूरी है ताकि सत्ता नहीं, संविधान सर्वोपरि हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन यह नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है। इसी कारण राज्यपालों की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यपालों को विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक निर्णय टालने से रोका है, जिससे यह बहस फिर तेज हुई है कि क्या यह पद सार्थक है?
एक और विकल्प यह हो सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के बजाय एक स्वतंत्र, बहुपक्षीय समिति करे। जिसमें सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा व लोकसभा के प्रतिनिधि और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की भी भूमिका हो। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सिर्फ एक राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का पुनर्संयोजन नहीं है, बल्कि पूरे भारत के संघीय ढांचे की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक साहसी हस्तक्षेप है। एक ऐसा संदेश जो राज्यपालों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी गहराई से समझना होगा।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।