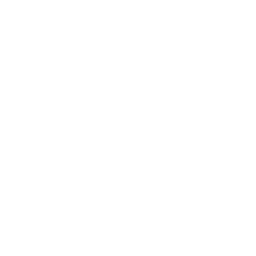आज की पीढ़ी में ये तूफान सा क्यों है...
आजकल हम अपने आसपास नजर डालें तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब युवाओं व आम लोगों में संघर्ष, टकराव व हिंसा की घटनाएं न होती हों। स्कूल-कालेजों में छात्रों की हिंसक लड़ाई, सड़क पर रोडरेज की घटनाएं, परिवार में हिंसा के दंश आम हो चले हैं। व्यवहार में आक्रामकता के चलते जरा-जरा सी बात में आत्मघात। रिश्ते जल्दी बनाने और जल्दी तोड़ने की प्रवृत्ति। इसी आक्रामकता के चलते कई तरह के मनो-शारीरिक रोग पैदा हो रहे हैं- मसलन उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, मधुमेह व हृदय रोग। आक्रामकता में हमारे विचार तत्व व मनोभावों की बड़ी भूमिका होती है। असहिष्णुता व आक्रामकता के निदान और उससे उपजे रोगों के उपचार में योग,प्राणायाम व ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंजाब वि.वि. की विवेकानंद पीठ में योग विभाग के प्रमुख आचार्य बलविंदर ने अरुण नैथानी से बातचीत में ऐसे ज्वलंत सवालों के जवाब दिए।
शहरयार का फिल्म ‘गमन’ के लिखा बहुचर्चित गीत ‘सीने में जलन आंखों में ये तूफान सा क्यों है’ हकीकत में नजर आ रहा है। जिधर देखो लोगों के व्यवहार में आक्रामकता ही आक्रामकता है। दरअसल, हम ही ऐसा समाज रच रहे हैं। स्कूल में दाखिल होते ही बच्चे पर अभिभावक व टीचर फर्स्ट आने का दबाव बना देते हैं। दरअसल, हम बच्चों को सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा सिखा रहे होते हैं। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। हरेक की अपनी सीमाएं हैं। यहीं से असंतुष्टता-असहनशीलता का बीजारोपण होता है। यही प्रतिस्पर्धा माध्यमिक स्कूलों,कालेजों व व्यावसायिक संस्थानों के छात्रों के व्यवहार में बढ़ती है। कालेज से निकलकर उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए फिर कंपीटशन होता है। सबको पछाड़कर आगे निकलना है। बात यहीं खत्म नहीं होती, शिक्षण संस्थान से निकल अच्छी जॉब, मोटे पैकेज के लिये प्रतिस्पर्धा। फिर कंपनी के टारगेट के दबाव व विभागीय स्पर्धा। फिर परिवार व मित्रों का दबाव कि कितनी संपत्ति जोड़ी, कितना कमाया। दरअसल, आज समाज में पैरामीटर बन गया कि येन-केन-प्रकारेण दूसरों को रौंदकर आगे बढ़ना है।
आक्रामकता से मानसिक विकृति तक
दरअसल, ये स्पर्धा जब तक समझ में आती है, चालीस-पचास के बाद ये मानसिक विकृति बन जाती है। चिंता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता हमारा स्वभाव बन जाता है। निस्संदेह, यह अप्रकृतिक है। संघर्ष हमारा स्वभाव बन जाता है। मन को अप्राकृतिक ढंग से चलाने से शरीर पर घातक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक क्षमताओं का शोषण होता है। जल्दी थकावट आती है। हमारी भागदौड़ से अनिद्रा, उच्च रक्तचाप व हृदयरोग में इजाफा होता है। किसी भी छात्र या कर्मचारी के टारगेट पूरे नहीं हुए तो हारने का, पीछे रहने का डर पैदा होता है। यह अवसाद, उदासी व भय का स्वभाव पैदा करता है। असहनशीलता हमारा स्वभाव बनने लगता है। इसकी छाया में उदासी आती है। ऐसे में बेचैनी का होना स्वाभाविक है। जिससे क्रोध व हिंसक भावना पैदा होती है।
मैत्री, करुणा और सम्मान जरूरी
ध्यान से देखें तो सामाजिक सहनशीलता- समाज, परिवार व दोस्तों में मैत्री, सहयोग, करुणा, सम्मान के भाव से पैदा होती है। इन गुणों से ही हमारा समाज-परिवार सहनशीलता के आधार पर चलेगा। हकीकत में हम इन गुणों को महत्व नहीं देते। दोस्तों में सहनशीलता नहीं है। आत्मघात की प्रवृत्ति बढ़ी है। एक-दूसरे के प्रति हिंसक हुए हैं। एक-दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। ये क्रोध व वैमनस्य पैदा करते हैं।
प्राचीन शिक्षा के संस्कार
वक्त की मांग है कि हम मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम छात्रों के विकास के प्रति सचेत रहें। स्कूल से ही बच्चों को मैत्री, करुणा व सहयोग सिखाएं। थोड़ा-बहुत स्पर्धा जरूरी है। मगर इसे प्रतिष्ठता का मुद्दा न बनाएं।
हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति के जरिये छात्रों में योग, ध्यान, धैर्य, मैत्री का भाव कूट-कूट कर भरा जाता था। छात्रों को प्रकृति के सान्निध्य में रहने को कहा जाता था। उन्हें नदी,झील, पहाड़ व मंदिर जाकर गुरु के सान्निध्य में योग-प्राणायाम सिखाते थे। एक-दूसरे के प्रति सम्मान व ईमानदारी का भाव जगता था। विशेष रूप से गुणों के विकास पर ध्यान दिया जाता था। आज चिकित्सा बिरादरी के सामने आक्रामकता के केस बढ़ रहे हैं, अब चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद या अन्य चिकित्सा पद्धति हो। वे भी चाहते हैं कि समाज में ध्यान बढ़े। जो मानवीय मूल्यों का आधार बनता है।
दरअसल, आज संघर्ष जीवन के हरेक क्षेत्र में है। फास्ट फूड की संस्कृति है। खाना जल्दी बन जाए और जल्दी खा लें। अब चाहे इंटरनेट हो, गाड़ी चलाना हो, कमाना हो हर तरफ तेजी चाहिए। विडंबना ये कि संबंध बनाने व तोड़ने में तेजी है। तब तेजी से तो धैर्य की जगह अधैर्य ही आएगा। दुष्परिणाम असहनशीलता के रूप में है। हमें प्राचीन मानवीय मूल्यों की तरफ लौटना होगा। लोग फिर थोड़ा प्राकृतिक व्यवहार की तरफ लौटें। हम अपने भीतर अप्राकृतिक, अधैर्य व हिंसक प्रवृत्ति को देखें। हम दूसरों में देखते हैं अपने आप में नहीं देख पाते। हम शुरुआत खुद से करें। अपना निरीक्षण करें। यदि अति स्पर्धा है तो उस पर नजर रखें। तब ही उसका निदान मिलेगा।
खानपान-व्यवहार में बदलाव
हम जीवनचर्या में अनुकूल परिवर्तन की पहचान करें। चिकित्सा वर्ग व समाज विज्ञानी मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति समाज में चेतनशीलता लाएं। नियमित रुप से सैर करें,जो भी समय मिले अब चाहे सुबह हो या शाम। खाना हल्का हो ताकि मन व शरीर पर अतिरिक्त भार न पड़े। स्वयं के भीतर की कमी मनन करें।
योग-ध्यान-प्राणायाम से उपचार
विशेषकर हमारी आक्रामकता के उपचार में ध्यान महत्वपूर्ण है। जिसे अच्छे संस्थान या योग टीचर से सीखें। नियमित रूप से किया करें। सप्ताह में परिवार के साथ बाहर प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन के लिये जाएं। प्रकृति की धीमी नैसर्गिक गति होती है। नदी, वन व झील दर्शन का प्रभाव पड़ता है हमारे अंतर्मन पर।
प्राणायाम लाभकारी
आम आदमी के लिए ध्यान -प्राणायाम करने का उद्देश्य मनो-शारीरिक स्वास्थ्य बनाये रखना है। ताकि शरीर के अंग ठीक से काम करें। मन में संतुलन, मैत्री, करुणा, सहयोग का भाव हो। प्राणायाम में अनुलोम-विलोम व भ्रामरी बेहद उपयोगी हैं। आसानी से कहीं से भी सीखे जा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम मनो-शारीरिक रूप से गहरी संतुष्टि देता है। शिथिलता व धैर्य प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से बीस बार करें, दस मिनट तक।
ध्यान का योगदान
दुनिया में अब हर जगह ध्यान को प्राथमिकता दी जाती है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिये साधारण ध्यान की जरूरत है। सबसे पहले गाइडेड मेडिटेशन करें। विपश्यना ध्यान में- श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। विपश्यना में श्वास का आना-जाना देखना है। ऐसा न हो कि श्वास में ध्यान व मन कहीं और हो। ध्यान पर सांस केंद्रित करने से एकाग्रता बढ़ती है। विपश्यना में ‘वि’ यानी विशेष, पश्यना माने आंतरिक दृष्टिकोण। महात्मा बुद्ध व बुद्ध के अनुयायियों के मार्गदर्शन में इसकी रचना की गई।
आसन भी जरूरी
अच्छे संस्थान व टीचर से आसनों का प्रशिक्षण लें। असहनशीलता का शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बीपी, अनिद्रा व चिंता रोग दूर करने में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान तो है, लेकिन आसन का भी बड़ा रोल है। चार प्रकार के दो-दो आसन नियमित करें। इससे कई मनो-शारीरिक रोग ठीक हो सकते हैं। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च दर्जे की हो जाती है। शारीरिक व मानसिक रूप से सहनशक्ति बढ़ती है।
कौन से आसन करेः-
Advertisement1. खड़े होकर आसन ताड़ आसन, कटिचक्र आसन- तीन से पांच बार रिपीट करें।
2. सीधे (लेटकर) –उत्तानपाद आसन, पवनमुक्त आसन और सेतुबंध आसन।
3. उलटे (पेट के बल) – सर्पासन, शलभ आसन- तीन से पांच बार रिपीट।
4. बैठकर –तितली आसन, वक्रासन ,उष्ट्रासन नियमित करें।नियमित रूप से योग्य गुरु के मार्गदर्शन में गहन श्वसन व अनुलोम-विलोम तथा भ्रामरी प्राणायाम करें। इस तरह विचारों के नियमन, संतुलित भोजन, आसन, प्राणायाम, ध्यान और जागरूकता से हम अपने व्यवहार की आक्रामकता पर अंकुश लगा सकते हैं। साथ ही स्वस्थ्य जीवन पा सकते हैं।